Ek pratidhwani ke liye
Material type: TextPublication details: New Delhi Vani 2024Description: 180pISBN:
TextPublication details: New Delhi Vani 2024Description: 180pISBN: - 9789362876515
- H 891.43033 SIN
| Item type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Gandhi Smriti Library | H 891.43033 SIN (Browse shelf(Opens below)) | Available | 180673 |
एक प्रतिध्वनि के लिए : अपने समय को जीते हुए उसे रचने की कला हर कवि में नहीं होती क्योंकि इसके लिए जिस गहन दृष्टि, सोच, संवेदना, सरोकार और जोखिम उठाने हेतु साहस की ज़रूरत, वह सबके बूते की बात नहीं। लेकिन ये सारे उतजोग श्याम सिंह के एक प्रतिध्वनि के लिए संग्रह में अगूढ़ देखने को मिलते हैं जो अपने आप में अनन्य। इस संग्रह की कविताओं को चार खण्डों में बाँटा गया है¬– 'समय की दीवार पर', 'झाँकने लगे हैं नये पत्ते', 'प्रेम के अभिप्राय सारे' और 'तुम ईश्वर क्यों बन गये, राम!' खण्ड ‘समय की दीवार पर' में कवि नित्य बदलते समय, समाज और व्यवस्था में जीवन-यथार्थ को जिस अन्वेषणात्मक प्रक्रिया से गुज़रते हुए पूरी दृश्यात्मकता के साथ दर्ज करता है, वह अपने कथ्य, भावों के घनत्व और भाषिक संरचना में प्रभावित तो करता ही है, कई बार अनेक सवालों के साथ संवाद को गहरे छू ठहर भी जाता है जिसका सशक्त उदाहरण पेश करती हैं 'दीवारें', 'शहर परिचित हो चला है', 'दुकान नुमाइश में मैंने भी लगायी', 'साहब, रेवेन्यूवाले जल्दी निकल लेते हैं', 'जंगल की लकड़ियाँ', 'राजा ने तन्ने नहीं जने', 'अक्सर समूह में ही चलती हैं लड़कियाँ', 'हिन्द के सलोने! समझो अपना किरदार', 'सूख गये आँसू उसकी ही आँखों में', 'तुम निष्ठावान हो!' 'क्रान्ति के बीज' जैसी कविताएँ। खण्ड 'झाँकने लगे हैं नये पत्ते' में प्रकृति-सम्बन्धी कविताएँ हैं जो प्रकृति के विभिन्न आयामों से होते हुए उसके उपादानों का आख्यान रचती हैं और बताती हैं कि हम अपनी सांस्कृतिकता में मूल और मूल्यों से कितने जुड़े हुए, कितने कटे हुए। ये हमारी संवेदना को अपने सूक्ष्म-से-सूक्ष्म तन्तुओं के ज़रिये भी कुन्द होने से बचाये रखने वाली रचनाएँ हैं। इस खण्ड की 'ओ क्षिप्रिके!', 'नये पत्ते' और 'गिलहरी' तो अप्रतिम हैं। वहीं 'प्रेम के अभिप्राय सारे' खण्ड में कवि ने प्रेम के छोह-विछोह का जो अनुभूत संसार रचा है, वह एक भिन्न क़िस्म की ताज़गी तो लिये हुए है ही, अपने पाठ और आस्वाद में कई बार अनदेखे, अनछुये की प्रतीति भी कराता है। इन कविताओं में कहीं भी कल्पना का अतिरेक नहीं बल्कि अपनी ज़ीस्त की अपनी दास्तान हैं ये, जिनकी बयानगी में सहचर समय और समष्टि भी एक मर्मी बनकर शामिल। इस परिदृश्य में 'मैं अब भी वहीं हूँ', 'तुम्हारे शोध में प्रतिबद्ध', 'आत्महत्या’, ‘खुद्दार है मेरा प्यार’, ‘कश्ती में बशर्ते तुम रहो', ‘उसे है मेरा इन्तज़ार', ‘यादों का अनुक्रम रहने दो', 'नहीं लिखूँगा', 'लत तेरी बेहिसाब यादों की लग गयी' उल्लेखनीय हैं। इस संग्रह का अन्तिम खण्ड है 'तुम ईश्वर क्यों बन गये, राम!' इसमें कवि ने राम को ईश्वर नहीं एक मनुष्य के रूप में देखने-समझने की जो दृष्टि रची है, उससे कविता का लोक बहुत बड़ा हो जाता है। यह पूरा खण्ड मिथकीय प्रतीकों से भरा है, लेकिन कवि का मानवीय पक्ष ही सबसे बड़ा है। चाहे वह ईसा मसीह की बात हो, भीष्म, कृष्ण या राम की, उसने किसी शून्य में विचरे बिना या जड़ताओं से बिना बँधे अपने युगकाल के अनुसार कथ्य को मूर्त करने की सोच और सम्बद्धता का परिचय दिया है। इसे 'निकल आओ, प्रभु! धर्मग्रन्थ से बाहर', 'कठघरे में भीष्म', 'राम! क्या सच में थे तुम?', 'तुम भाग्यशाली थे कृष्ण’ रचनाओं में सहज ही लक्षित किया जा सकता है। निस्सन्देह, श्याम सिंह का यह संग्रह अपने समय की संगत में रचा गया एक ऐसा संग्रह है, जिसकी यात्रा में संवाद के लिए सवाल जाने कितने, लेकिन मौन ही हर तरफ़ ज़्यादा; जब कि कवि निरन्तर प्रतीक्षारत एक प्रतिध्वनि के लिए!
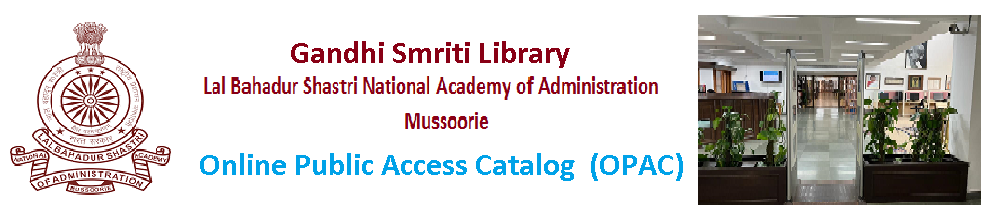

There are no comments on this title.