Shurveer yodha : hamare margdarshi sidhant
Material type: TextPublication details: New Delhi Central Reserve Police Force 2021.Description: 41 pSubject(s): DDC classification:
TextPublication details: New Delhi Central Reserve Police Force 2021.Description: 41 pSubject(s): DDC classification: - H 355.13323 SHU
| Item type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Donated Books
Donated Books
|
Gandhi Smriti Library | H 355.13323 SHU (Browse shelf(Opens below)) | Available | 172099 |
बीते 2000 वर्षों में इस बात के लिए कोई तर्क नहीं मिल पाया है कि, जब युद्ध लड़ना ही है तो उसे सुनियोजित तरीके से क्यों न लड़ा जाए।" टी ई लॉरेंस का यह कथन, युद्ध के मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए जाने की आवश्यकता को इंगित करता है। सन जू ने द आर्ट ऑफ चॉर में ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांतों को नैतिक प्रभाव, मौसम, भूभाग और कमान के साथ युद्ध के पांच मूलभूत कारकों में से एक माना है। हालांकि, आंतरिक सुरक्षा तंत्र पर नए कुटिल या विभिन्न गैर-सैन्य (हाइब्रिड) तरीकों से आक्रमण करने के वर्तमान युग में युद्ध के पारंपरिक मार्गदर्शी सिद्धांतों में सुधार और परिवर्तन करना जरूरी हो गया है। इसलिए, राष्ट्रीय हित के विभिन्न नियंत्रकों अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा का दृष्टिकोण संभावित खतरे सरकार की नीतियां और निर्णय; अनुभव; लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत नागरिक समाज के अधिकार क्षेत्र की गतिशील विशेषताओं आदि का महत्व बहुत बढ़ गया है। भूभाग के बजाय स्थानीय लोगों की उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित किया जाना और सैन्य वर्चस्व के साथ नागरिक जीत का संलयन किया जाना एक उल्लेखनीय बदलाव है।
मार्गदर्शी सिद्धांत विचार से कर्म तक पहुंचने का सेतु होता है कुछ हद तक कालातीत होता है और ऐसा बौद्धिक घटक होता है जिसके आधार पर स्थितिगत अनुभवों से पैदा हुए विभिन्न तीव्रता वाले संघर्षों में शांति बहाल किए जाने के नियम बनाए जाते हैं। इसे एक ऐसा व्यावहारिक और गतिशील घटक भी माना जाता है जिसके आधार पर, उभरते रुझानों के विश्लेषण में पूर्वानुमान लगाने के अलावा उग्र सुधारवादी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उच्च तीव्रता वाले संघर्षों के समाधानों संबंधी नियमों की व्याख्या की जा सकती है और यह भी तय किया जा सकता है कि युद्ध के लिए उपयोगी जनमानस या स्थानीय आबादी के बोध की दिशा बदलने के अलावा भविष्य में शारीरिक बल का उपयोग कैसे किया जा सकता है।
इसी संदर्भ में लंबे समय से यह अपेक्षा की जा रही थी कि हमारे मार्गदर्शी सिद्धांतों को भी लेखबद्ध किया जाए। हालांकि, हम कट्टर सिद्धांत बनाए जाने के बिलकुल पक्षधर नहीं हैं, बल्कि हम उन्हें मार्गदर्शी और परामर्शी स्वरूप देना चाहते हैं, जिन्हें न केवल समय के साथ-साथ अद्यतन किया जाए बल्कि आवश्यक होने पर बदला भी जाए। हमारे मार्गदर्शी सिद्धांतों में नियमों, जडसूत्रों और दिशानिर्देशों का समावेश तो है लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि (इंटर ऑपरेबलिटी) को सुनिश्चित करने के लिए इनमें मानकीकृत टीटीपी (रणनीति, तकनीक और कार्यविधि) को भी शामिल किया जाए।
हम, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल रूप में, दुनिया के सबसे बड़े, वस्तुतः अधिकांश सुरक्षा बलों से भी बड़े अर्धसैनिक बल हैं, और इसीलिए हमें जल्द से जल्द अपने मार्गदर्शी सिद्धांतों में परिशोधन करने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसा करके ही हम कहीं भी और कभी भी संज्ञानात्मक कार्यसाधन के माध्यम से बदलाव लाने की शक्ति प्राप्त कर पाएंगे और उसके माध्यम से आधुनिक युग की प्रौद्योगिकी से जुड़े वैश्विक समाज के विराट परिदृश्य को संबोधित कर पाएंगे।
इस बात में कोई दो राय नहीं हैं कि प्रौद्योगिकी हमें सशक्त बनाती है, लेकिन इस बात को भी स्पष्ट रूप से समझ लिया जाना जरूरी है कि अंतत: "लड़ने की चाह ही वह सबसे महत्वपूर्ण कारक है, जिसकी उपेक्षा करने पर रणनीति या युद्ध कौशल भी व्यर्थ या विफल हो सकते हैं। हमें, के.रि.पु.बल योद्धाओं को लड़ने के लिए तथा देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत राष्ट्र कल्याण से जुड़े किसी भी ध्येय को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। और, इसीलिए, समय आने पर हम सभी में जीत की ललक पैदा करने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए "शूरवीर योद्धा को हमारी रणनीति का एक अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए ।
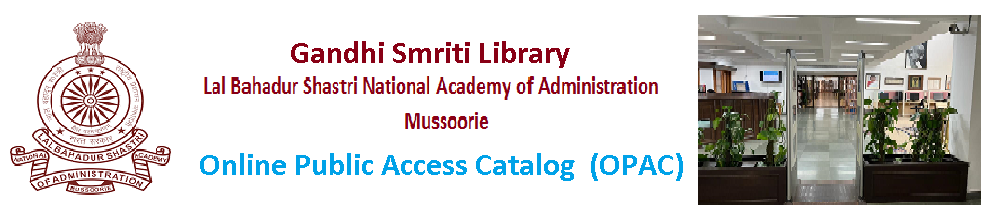
There are no comments on this title.